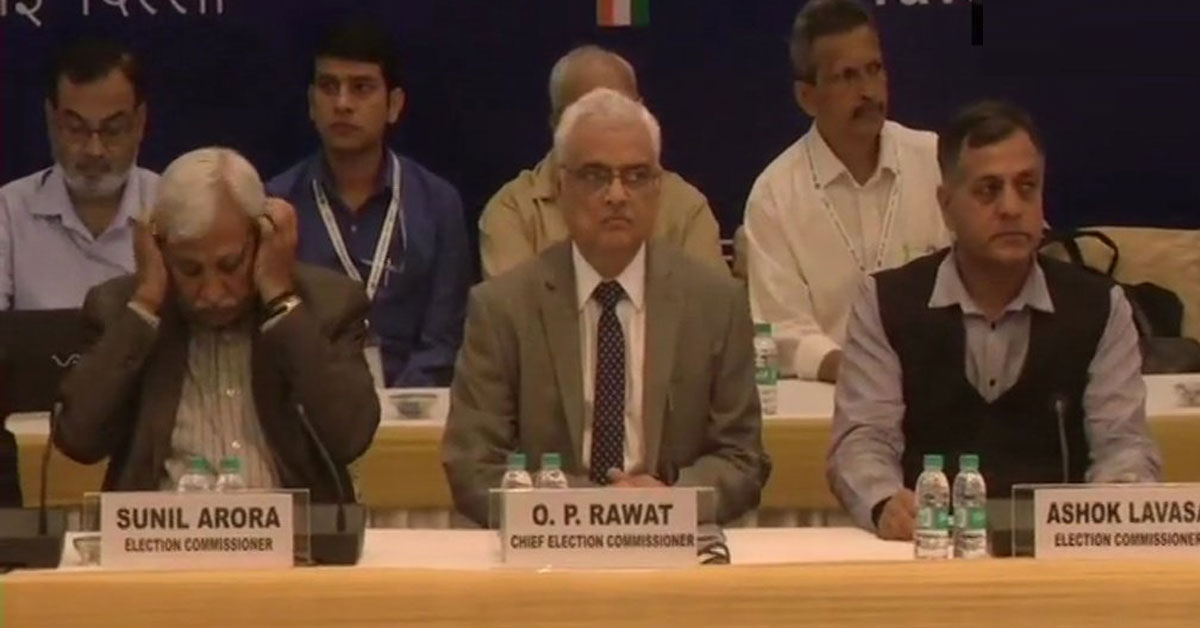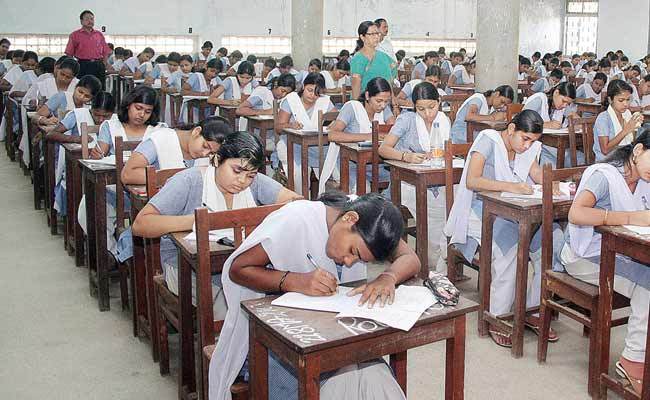दिहाड़ी मजदूरों पर विशेष ध्यान की जरूरत

– गिरीश्वर मिश्र
पिछले कुछ समय से पूरे देश के लिये हुक्म है कि घर में बंद रहो और यह जीवन की रक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिये लिया गया सरकारी निर्णय है जिसका सब ने मान रखा। पर घर-बैठकी का अर्थ गरीब और अमीर या फिर पक्की नौकरी वाले जो महीने-महीने तनख्वाह उगाहते हैं सबके लिये एक सी नहीं हुआ करती। जो रोज कमाते खाते हैं, उनकी मुसीबत सबसे ज्यादा है। इन्तजार करते दिन, हफ्ते और महीने बीते और उनका दिन ही शुरू नहीं हो रहा है। जिस छोटे-मोटे काम से उनका निर्वाह होता था वहां भी तालाबन्दी है और इस विकट घड़ी में कुछ भी सूझ नहीं रहा है। उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनका कसूर क्या है और उनकी किस गलती से उनकी रोजी-रोटी छिन गई।
ऐसी बेहाली में इन गरीबों को सोचना पड़ा कि महामारी बड़ी या पेट की भूख? मरने के लिए भी तो जीना जरूरी है, आखिर भूख से मरने के बाद बीमारी किसको मारेगी? सो इन दिहाड़ी मजदूरों के सामने कोई और विकल्प नहीं बचा, सिवाय इसके कि वे वापस अपने-अपने गाँव जायें और नए सिरे से गुजर बसर करने का कुछ उपाय करें। जिन्दगी और मौत के संशय में लाकडाउन की परवाह न करते हुए वे गाँवों की ओर कूच कर दिए। लाखों की तादात में ये मजदूर सैकड़ों मील दूर की मंजिल की ओर चल पड़े। लोकतंत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता है और उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, सो अपने सीमित संसाधनों से इनकी लम्बी यात्रा शुरू हुई। सरकार और विपक्ष दोनों ही परिस्थिति का जायजा लेते रहे, द्रष्टा बने रहे, कानून और व्यवस्था के नाम पर मनमर्जी करते रहे और भूखे-प्यासे मजदूर वर्ग का कारवां चलता रहा।
आरम्भ में सरकारी व्यवस्था में विशाल जनप्रवाह को रोकने की न मंशा थी न व्यवस्था ही थी। पर बढ़ते दबाव के बीच कुछ करने के लिए बाध्य होना पड़ा। रहने-खाने की कुछ व्यवस्था शुरू हुई। फिर बसों से पहुंचाने का दौर शुरू हुआ। अगले चरण में ट्रेनें चली, जिसे लेकर केन्द्र और प्रदेश सरकारों के बीच जो तनातनी हुई वह अभी बरकरार है। ट्रेनों का आना-जाना विलक्षण ढंग से हो रहा है। सरकारी खींचतान के बीच उनका चलना ही मुश्किल होता है और जो चल भी रही हैं तो अपने गन्तव्य तक पहुंचने में तीन गुना समय ले रही हैं और उसमें जरूरी सुविधाएँ भी नहीं रह रही हैं। गिरते-पड़ते गांव पहुंचने पर उन्हें कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।
यह सही है कि स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं पर जिस स्थिति से ये गरीब गुजर रहे हैं, उनसे बचा जा सकता है और परिस्थति को बेहतर बनाया जा सकता है। कई जगह अधिकारियों और आम जनता की अच्छी पहल की खबरें भी आ रही हैं। परन्तु व्यापक नीतिगत प्रश्न मुंह बाए खड़े हैं। इन सबके बीच राजनीति का चरित्र भी श्वेत-श्याम अपने सभी रंगों के साथ उभरा। पता चला राजनीति सिर्फ राजनीति होती है और मानवता के प्रश्न भी उसी दायरे में निपटाए जाएंगे। बहुत से मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ उखाड़ फेंकने की अनुभूति लेकर लौट रहे हैं और उन्हें कुछ सूझ भी नहीं रहा है।
मजदूरों का पलायन नियमित रूप से जारी है किन्तु लाखों की संख्या में श्रमिकों की स्थिति, उनके श्रम के योगदान और समाज में उनके स्थान को लेकर कोई सोच नहीं बन पा रही है। गावों में उनके स्वास्थ्य, पुनर्वास और वापसी को लेकर गंभीरता से कोई विचार-विमर्श नहीं हो रहा है। इस कठिन समय में राजधर्म की एक ही पुकार है कि राजनीति को मुल्तबी रखकर जीवन की लौ जलाए रखने की युक्ति सोची जाय। खट्टे मन और क्षोभ के साथ लुटे हुए जैसी अनुभूति लिये हुए इन परिवारों की भावना और आवश्यकता को समझ कर सहयोग देना जरूरी होगा। इस हेतु गाँव को विकास की रणनीति में वरीयता देनी होगी।
लॉकडाउन खत्म होने के साथ मजदूरों की वापसी की व्यवस्था खड़ी हो रही है। स्वास्थ्य और आजीविका का संतुलन बनाना कठिन चुनौती है। बड़े उद्योगों में इन मजदूरों की भूमिका महत्वपूर्ण है और औद्योगिक विकास को गति देना भी जरूरी है। प्नधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। इस उद्देश्य को चरितार्थ करने में इन दीन-हीन मजदूरों की बड़ी भूमिका होगी। असंगठित क्षेत्र में श्रम के मूल्य को प्रतिष्ठित करना बड़ी चुनौती है, जिस ओर ध्यान कम ही जा पाता है। आशा है इनकी भी सुनी जायगी और आर्थिक नियोजन में उचित स्थान मिलेगा।
(लेखक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विवि, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)